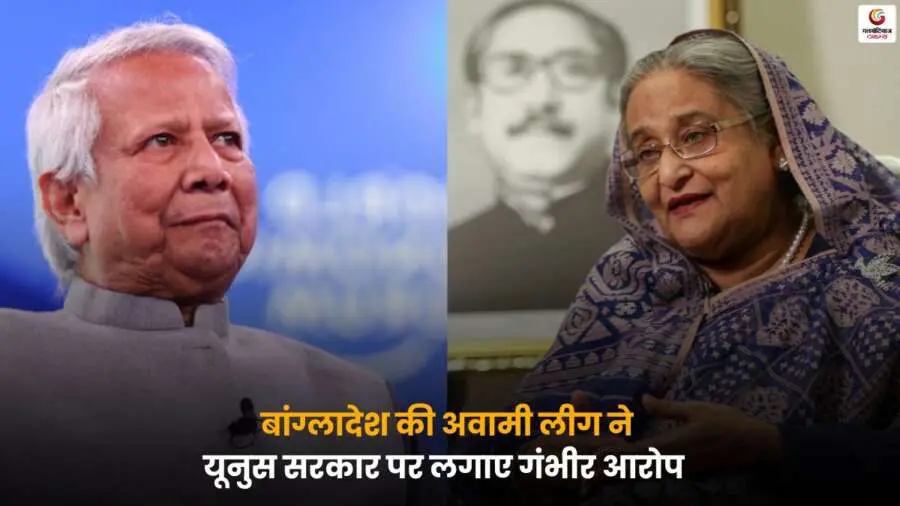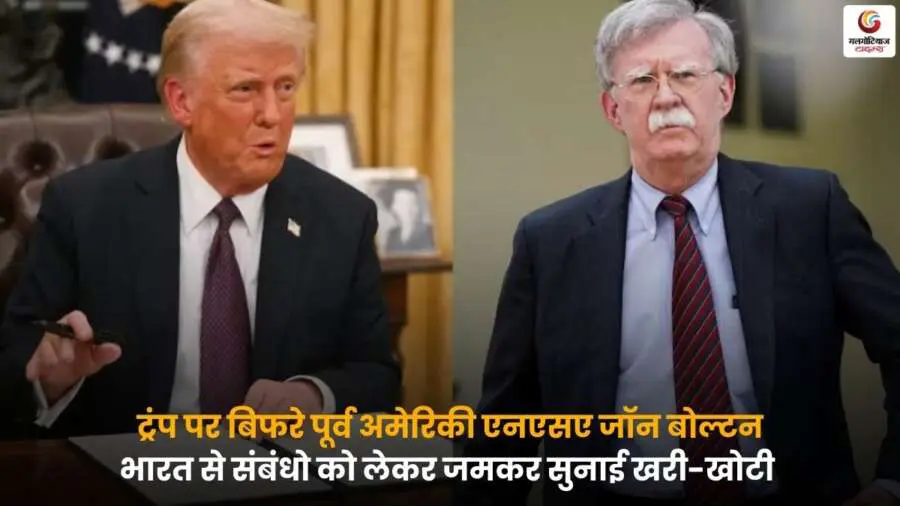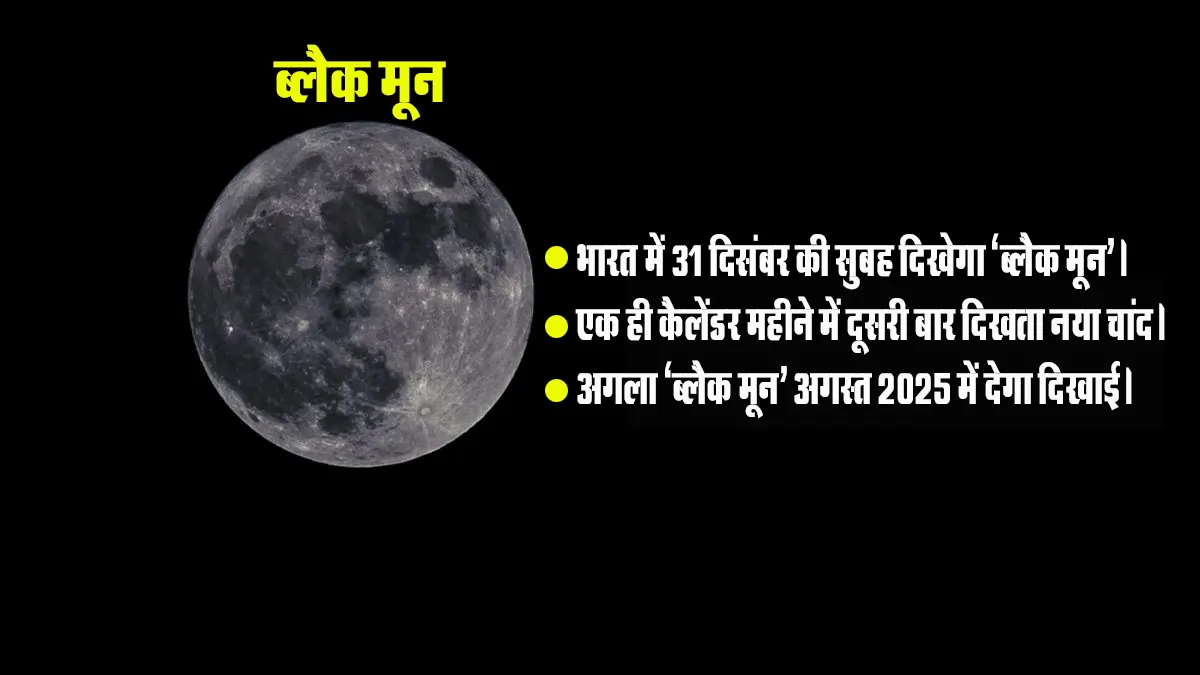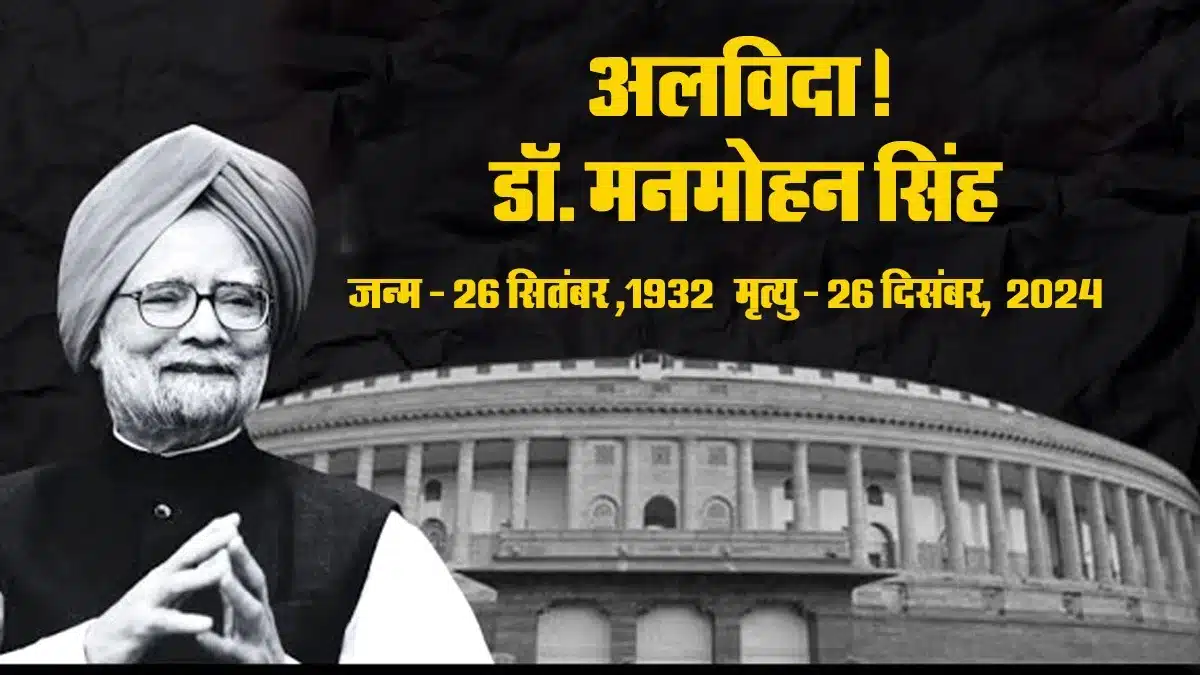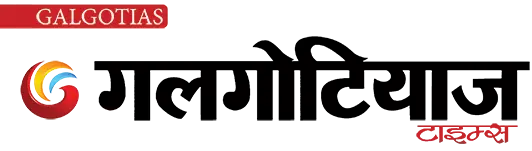नेपाल को चीन के आगे क्यों झुकना पड़ा? हर 5 साल में चढ़ावा भेजने की क्या थी मजबूरी?
Authored By: Nishant Singh
Published On: Wednesday, September 10, 2025
Last Updated On: Wednesday, September 10, 2025
19वीं सदी में नेपाल हर पांच साल में चीन को बहुमूल्य नजराना क्यों भेजता था? हाथी-घोड़े से लेकर सोना-चांदी तक, यह परंपरा नेपाल की मजबूरी और चीन की शक्ति का प्रतीक थी. 1855-56 के नेपाल-तिब्बत युद्ध और उसके बाद हुई संधि ने इसे जन्म दिया. आखिर किस शर्त ने नेपाल को झुकने पर मजबूर किया और कैसे यह अपमानजनक परंपरा खत्म हुई? जानिए नेपाल-चीन रिश्तों की वो अनकही कहानी, जिसमें इतिहास और राजनीति दोनों छुपे हैं.
Authored By: Nishant Singh
Last Updated On: Wednesday, September 10, 2025
दक्षिण एशिया का इतिहास सिर्फ़ राजाओं, महलों और युद्धों की गाथा नहीं है, (Nepal China Relations Compulsion) बल्कि यह कूटनीति, अधीनता और आत्मसम्मान की कहानियों से भी भरा पड़ा है. भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो आज अपनी स्वतंत्र पहचान और संप्रभुता पर गर्व करता है, कभी चीन के सामने इतना मजबूर था कि उसे हर पांच साल पर नजराना यानी कीमती तोहफे भेजने पड़ते थे. सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि 19वीं सदी में नेपाल ने एक संधि के तहत चीन को न केवल श्रद्धांजलि दी, बल्कि उसे अपने शाही दरबार में बाकायदा बहुमूल्य उपहार पेश करने की बाध्यता भी निभाई. सवाल उठता है कि आखिर नेपाल को यह अपमानजनक परंपरा निभानी क्यों पड़ी? किस युद्ध के बाद नेपाल इस स्थिति में पहुंच गया? और फिर यह परंपरा आखिर कब और कैसे समाप्त हुई?
नेपाल और तिब्बत: पड़ोसी लेकिन विवादों से घिरे संबंध
नेपाल और तिब्बत की भौगोलिक सीमाएं भले ही पहाड़ों से जुड़ी हों, लेकिन दोनों के बीच लंबे समय से मतभेद और टकराव चलते रहे. 18वीं और 19वीं सदी में नेपाल की गोरखा सेना बेहद शक्तिशाली मानी जाती थी. गोरखा योद्धाओं की बहादुरी और अनुशासन का डंका पूरे एशिया में बजता था. नेपाल ने कई छोटे-छोटे रियासतों को मिलाकर अपने राज्य का विस्तार किया. इसी महत्वाकांक्षा में उसकी नजर तिब्बत पर भी गई.
तिब्बत, जो उस दौर में चीन के क्विंग राजवंश के प्रभाव में था, नेपाल के लिए एक रणनीतिक क्षेत्र माना जाता था. नेपाल तिब्बत से व्यापार करना चाहता था और उस पर दबाव बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था. यही कारण बना 1855-56 के नेपाल-तिब्बत युद्ध का.
1855-56 का नेपाल-तिब्बत युद्ध
इस युद्ध की शुरुआत नेपाल की गोरखा सेना ने की. नेपाल ने दावा किया कि तिब्बत व्यापार में अनुचित रवैया अपना रहा है और नेपाल के व्यापारियों को परेशान कर रहा है. इसके अलावा नेपाल चाहता था कि तिब्बत उस पर आर्थिक रूप से निर्भर रहे.
नेपाल ने तिब्बत पर चढ़ाई कर दी. शुरुआत में गोरखा सेना ने तिब्बत के कई क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया. लेकिन तिब्बत चीन के अधीन था और वहां का संरक्षक क्विंग साम्राज्य खुद को चुनौती महसूस करने लगा. चीन ने तिब्बत की रक्षा के लिए दबाव बनाया और युद्ध की स्थिति को खत्म करने के लिए नेपाल से बातचीत कराई.
इस युद्ध ने नेपाल को यह एहसास कराया कि अकेले तिब्बत से भिड़ना आसान है, लेकिन चीन से टकराना भारी पड़ सकता है. और यहीं से जन्म हुआ उस संधि का जिसने नेपाल को पांच साल पर नजराना भेजने के लिए मजबूर कर दिया.
1856 की शांति संधि और नजराने की परंपरा
नेपाल और तिब्बत के बीच युद्ध के बाद 1856 में एक शांति संधि हुई, जिसे इतिहास में “नेपाल-तिब्बत संधि” के नाम से जाना जाता है. इस संधि की शर्तें नेपाल के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं थीं.
इस संधि में यह तय हुआ कि-
- नेपाल तिब्बत पर अपने सैन्य दबाव को खत्म करेगा.
- नेपाल को हर पांच साल में चीन के शाही दरबार में एक प्रतिनिधिमंडल भेजना होगा.
- इस प्रतिनिधिमंडल को सिर्फ औपचारिक अभिवादन नहीं करना था, बल्कि चीन को बहुमूल्य नजराना यानी हाथी, घोड़े, ऊन, धातुएं, सिक्के और अन्य कीमती वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट करनी पड़ती थीं.
- यह नजराना चीन की सर्वोच्चता और तिब्बत पर उसके प्रभुत्व को मान्यता देने का प्रतीक माना जाता था.
इस तरह नेपाल, भले ही औपचारिक रूप से स्वतंत्र रहा, लेकिन चीन के सामने अधीनता दिखाने पर मजबूर हो गया.
क्विंग राजवंश का प्रभाव और राजनीतिक खेल
उस दौर में चीन पर क्विंग राजवंश की सत्ता थी, जो एशिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था. तिब्बत चीन के लिए एक रणनीतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था. नेपाल और तिब्बत के बीच जब भी विवाद होता, तो चीन का वायसराय उसमें मध्यस्थता करता.
नेपाल को मजबूरी में चीन की सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ी. पांच साल पर भेजा जाने वाला यह नजराना चीन के लिए जीत का प्रतीक था और नेपाल के लिए अपमानजनक परंपरा.
नजराने में क्या-क्या होता था?
इतिहासकार बताते हैं कि नेपाल से चीन भेजे जाने वाले नजराने साधारण नहीं होते थे. इनमें शामिल थे:
- हाथी और घोड़े जैसे दुर्लभ जानवर
- ऊन और कपड़े
- कीमती धातुएं जैसे सोना-चांदी
- सिक्के और मूल्यवान वस्त्र
- नेपाल के कारीगरों द्वारा बनाए गए शिल्प
ये नजराने चीन के शाही दरबार में विशेष सम्मान के साथ स्वीकार किए जाते थे. लेकिन इसके पीछे छुपा संदेश यही था कि नेपाल चीन की अधीनता को स्वीकार कर चुका है.
अधीनता का प्रतीक या कूटनीति?
इतिहासकारों की राय इस पर बंटी हुई है. कुछ लोग मानते हैं कि यह नेपाल की मजबूरी और अधीनता का प्रतीक था. नेपाल के पास उस दौर में चीन से भिड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए उसने संधि को स्वीकार किया.
दूसरी ओर, कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि नेपाल ने इसे पूरी तरह अधीनता की तरह नहीं देखा. उनके अनुसार नेपाल ने इस नजराने को कूटनीति के तौर पर स्वीकार किया ताकि क्षेत्रीय शांति बनी रहे और चीन से सीधा टकराव टल सके.
नजराने की परंपरा का अंत
यह परंपरा ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली. इतिहास में दर्ज है कि नेपाल ने 1865 में आखिरी बार चीन को श्रद्धांजलि भेजी. इसके बाद नेपाल ने इस व्यवस्था को मानने से इंकार कर दिया.
समय के साथ नेपाल ने अपने संप्रभु राष्ट्र होने का दावा और मजबूत किया. चीन भी उस दौर में आंतरिक संकटों और विदेशी ताकतों के दबाव से जूझ रहा था, इसलिए वह नेपाल को नजराना भेजने पर मजबूर नहीं कर सका. इस तरह धीरे-धीरे यह परंपरा खत्म हो गई.
आज के संदर्भ में नेपाल-चीन संबंध
आज का नेपाल वही देश है, जिसने कभी हर पांच साल पर चीन के सामने सिर झुकाया था. अब हालात बदल चुके हैं. नेपाल आज एक लोकतांत्रिक देश है और चीन के साथ उसके संबंध साझेदारी और सहयोग पर आधारित बताए जाते हैं.
हालांकि चीन अभी भी नेपाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था में प्रभाव डालने की कोशिश करता रहता है. कई बार नेपाल की जनता इस दबाव के खिलाफ विरोध भी करती है, जैसा हाल ही में सोशल मीडिया बैन और विरोध प्रदर्शनों के दौरान देखा गया.
निष्कर्ष
नेपाल और चीन का रिश्ता इतिहास में अधीनता और नजराने से शुरू होकर आज रणनीतिक साझेदारी तक पहुंच चुका है. 1855-56 के तिब्बत युद्ध और उसके बाद हुई संधि ने नेपाल को पांच साल पर नजराना भेजने के लिए मजबूर कर दिया था. यह प्रथा चीन की सर्वोच्चता का प्रतीक थी, लेकिन नेपाल के आत्मसम्मान पर एक गहरा धब्बा भी.
आखिरकार नेपाल ने इस अपमानजनक परंपरा से छुटकारा पा लिया और अपनी संप्रभु पहचान कायम रखी. यह कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं, बल्कि हर उस छोटे राष्ट्र की है जो बड़े साम्राज्यों के सामने झुकने को मजबूर होते हैं, लेकिन वक्त आने पर अपनी स्वतंत्रता का परचम भी लहराते हैं.
ये भी पढ़ें:- नेपाल में राजनीतिक संकट: भारत-नेपाल संबंधों पर क्या होगा असर?