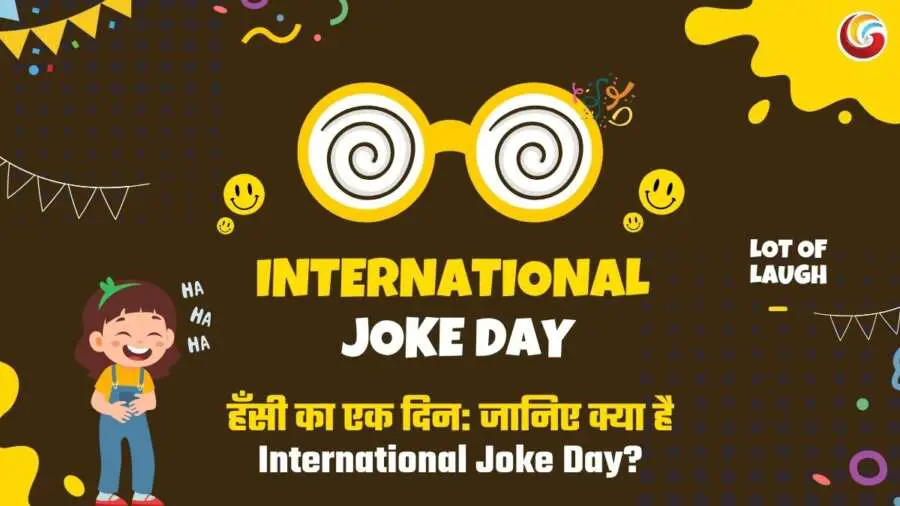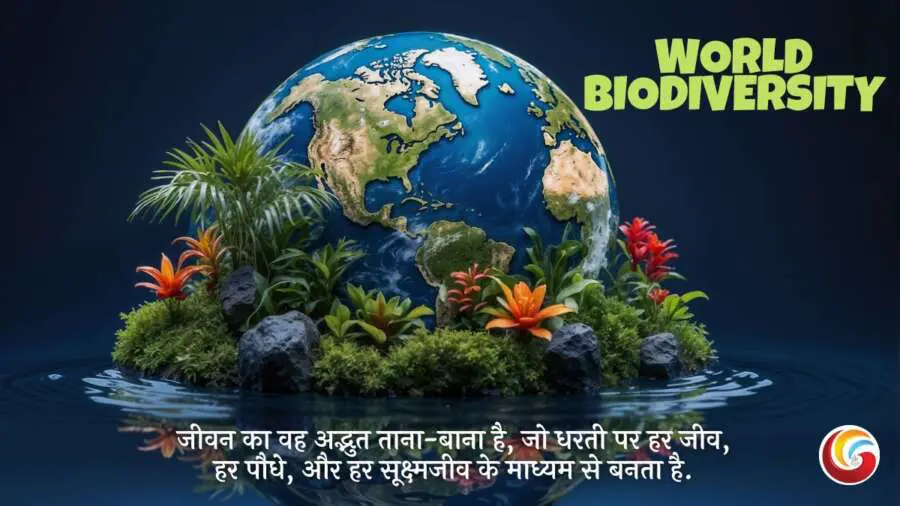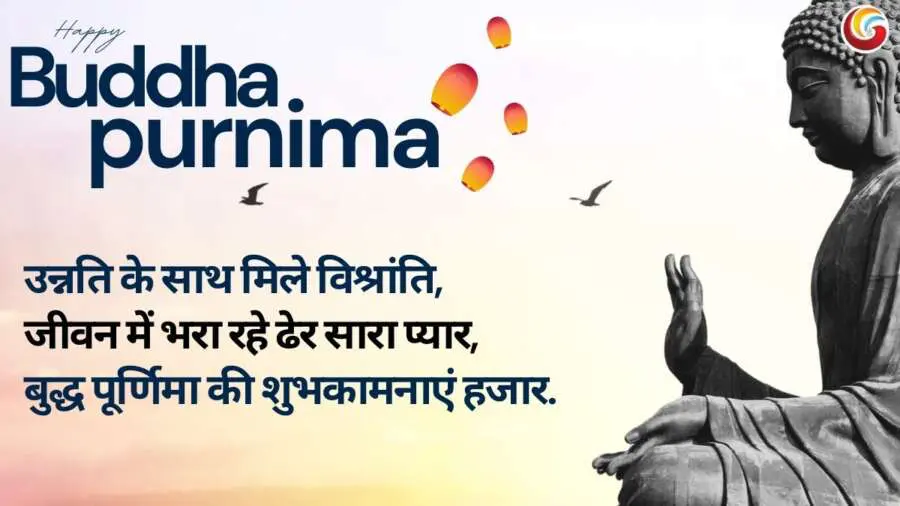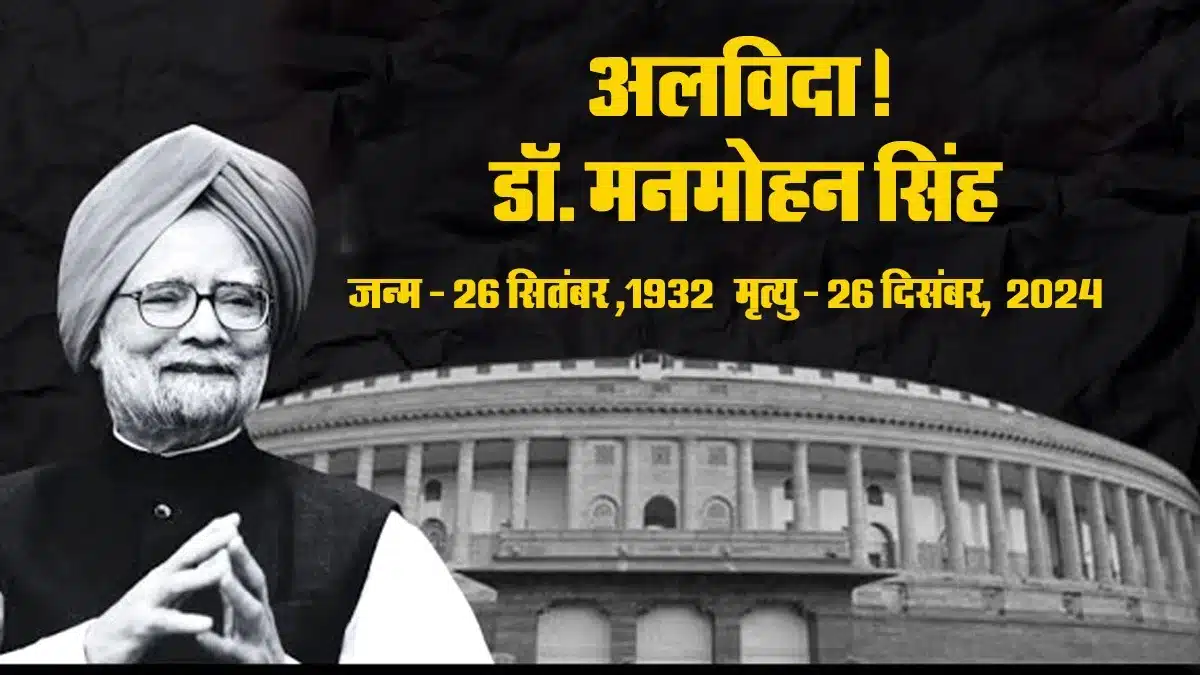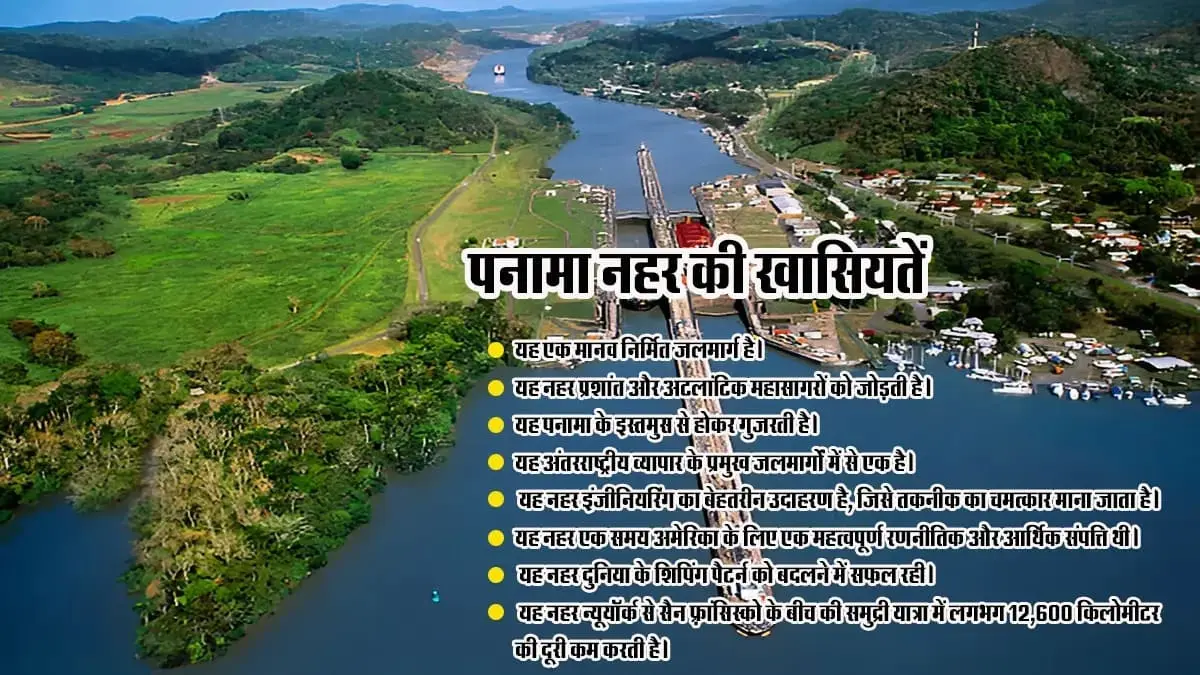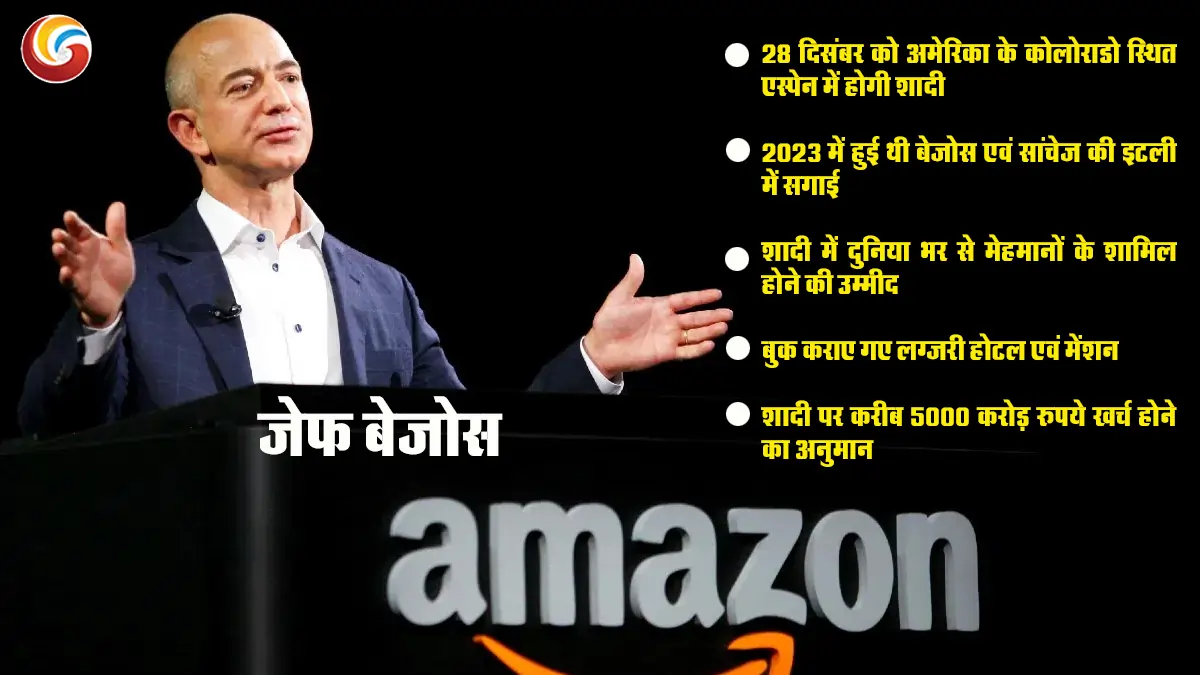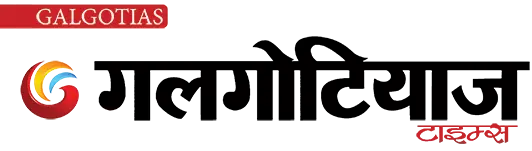Special Coverage
‘बुद्धा’ राइस के अवतार में फिर से छाया स्वाद एवं सुगंध का राजा ‘कालानमक चावल’
‘बुद्धा’ राइस के अवतार में फिर से छाया स्वाद एवं सुगंध का राजा ‘कालानमक चावल’
Authored By: अंशु सिंह
Published On: Monday, July 22, 2024
Last Updated On: Monday, July 22, 2024
'कालानमक चावल', जिसे 'बुद्धा राइस' के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर से लोकप्रियता हासिल कर रहा है। यह चावल अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे 'स्वाद एवं सुगंध का राजा' कहा जाता है।
Authored By: अंशु सिंह
Last Updated On: Monday, July 22, 2024
भारत में धान की हजारों प्रजातियां उपजायी जाती हैं। कृषि जितना पुराना धान का भी इतिहास रहा है। पुरातत्वविदों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की बेलन नदी घाटी में सबसे पुरानी जंगली चावल प्रजाति की खेती हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता में लोथाल में धान की खेती का जिक्र मिलता है। ऋगवेद में भले ही चावल का उल्लेख न मिलता हो, लेकिन यजुर वेद में ‘धान्य’ नाम से इसकी चर्चा है। रामायण एवं महाभारत में भी चावल का नाम आता है। हम सभी जानते हैं कि कैसे श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को अक्षयपात्र दिया था, जो सदैव चावल से भरा रहता था। इसी प्रकार, कालानमक चावल का इतिहास भी 600 ईसा पूर्व या गौतम बुद्ध काल से जुड़ा माना जाता है।
प्राचीन काल में यह चावल मूल रूप से उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के तराई क्षेत्रों में उगाया जाता था। कालांतर में यह विलुप्त होने लगा, जिसके बाद राज्य, केंद्र सरकार एवं कृषि वैज्ञानिकों ने इसे पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। आज उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में करीब 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती हो रही है। जापान, मलेशिया, कंबोडिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में इसका निर्यात भी किया जा रहा है। वर्ष 2021 में यूपी सरकार के ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट स्कीम’ के तहत कालानमक चावल को ‘बुद्धा होम राइस’ ब्रांड नाम से सिंगापुर निर्यात भी किया जा चुका है।
कालानमक चावल के आगे फीकी सारी प्रजातियां
अपने सुगंध, स्वाद एवं लंबे दानों के लिए मशहूर बासमती चावल भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति मानी जाती है। पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर उगाया जाने वाला यह चावल बिरयानी, पुलाव से लेकर कई पारंपरिक भारतीय व्यंजनों का एक प्रमुख घटक रहा है। लेकिन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में उगाये जाने वाले कालानमक धान से बने चावल के स्वाद एवं सुगंध के आगे बासमती भी फिकी पड़ जाती है। बावजूद इसके, आखिर क्यों यह चावल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया। जो कालानमक चावल किसी समय बनारस एवं अवध के राजसी रसोई की शान बढ़ाया करता था, वह थाली से गायब हो गया। स्मृति में रह गईं, तो सिर्फ उससे जुड़ी कहानियां एवं किस्से। हालांकि, बीते दो दशक में उत्तर प्रदेश सरकार एवं चावल अनुसंधान से जुड़े कुछ विशिष्ट कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से स्थिति कुछ बदली है। संयुक्त राष्ट्र के अलावा नाइजेरिया, कंबोडिया, फिलीपींस, म्यांमार, इंडोनेशिया आदि देशों में धान की खेती पर शोध करने वाले, पद्मश्री डॉ. आर.सी. चौधरी के अनुसार, देश की आजादी के समय जहां 50 हजार हेक्टेयर भूमि में कालानमक धान की खेती हो रही थी, वह 1990 के दशक के आते-आते 2000 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र में सिमट कर रह गई।
क्यों विलुप्त हुआ कालानमक चावल?

सवाल है कि आखिर क्यों किसान कालानमक धान की खेती से विमुख हो गए? इस बारे में पंतनगर के जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एवं पुसा के डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक और एम.एस.स्वामीनाथन के साथ काम कर चुके डॉ. राम चेत चौधरी का कहना है, ‘जैसे मरीज को जांचने के क्रम में डॉक्टर पहले बीमारी की वजह जानने का प्रयास करते हैं, वैसे ही मैंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर कालानमक की विलुप्ति का कारण क्या है? मुझे पता चला कि कालानमक की सुगंध एवं स्वाद (उसकी मूलायमियत) गायब होने से किसानों का मोह भंग-सा हो गया था। कालानमक की पैदावार कम एवं धीमी होने से उन्होंने उसे घाटे का सौदा समझा। कुछ लोग ही बचे, जो घाटे एवं फायदे का सोचे बिना कालानमक धान की पैदावार में लगे रहे। लेकिन वे अपने तरीके से इसकी खेती करते थे, न कि वैज्ञानिक तरीके से। वर्ष 1965 के आसपास ताइवान एवं फिलिपींस (आईआऱ8) से धान की नई वेराइटी आई। ये दोनों बौनी वेराइटी थीं, जिनसे काफी अच्छी पैदावार होने लगी। इन सबके अलावा कालानमक को लेकर कोई अनुसंधान नहीं हुआ, जिससे कोई नई प्रजाति नहीं निकली और वह विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई। कुछ किसानों का यह भी कहना है कि ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों के अत्याचार के कारण उनके पूर्वज इसे उगाने से कतराने लगे थे।‘
गौतम बुद्ध की झोली से निकला धान
कालानमक धान के अनुसंधान से जुड़े डॉ. राम चेत चौधरी बताते हैं कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल है, जिसका इतिहास गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। जब गौतम बुद्ध बिहार के बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् अपने पिता की राजधानी कपिलवस्तु (वर्तमान में सिद्धार्थनगर के पिपरवाह एवं नेपाल के कपिलवस्तु जिले के बीच स्थित स्थान) लौट रहे थे, तो रास्ते में बजहा नामक स्थान पर उनका रुकना हुआ। अगले दिन जब वे गांव से जाने लगे, तो ग्रामीणों ने उनसे आशीर्वाद देने को कहा। तब भगवान बुद्ध ने अपनी झोली में से एक मुट्ठी धान निकालकर दिया और कहा कि वे निचली जमीन में इसकी खेती करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस धान से जो चावल तैयार होगा, उसकी सुगंध हमेशा उनकी याद दिलाएगी, जबकि इसमें मौजूद पोषक तत्व उनका प्रसाद होगा। इस तरह बजहा, मथला गांव में इसकी रोपाई की गई और कालांतर में वह कालानमक चावल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तब से यह भगवान बुद्ध के महाप्रसाद के रूप में जाना जाता है।‘ इस वाक्ये का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र के फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) द्वारा प्रकाशित ‘स्पेशलिएलिटी राइस ऑफ द वर्ल्ड’ किताब के अलावा ‘कालानमक धान : अतीत से वर्तमान’ एवं ‘स्टोरी ऑफ कालानमक राइस’ पुस्तक में भी मिलता है।
डॉ. चौधरी बताते हैं कि पांचवीं शताब्दी की शुरुआत में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे, तो उन्होंने भी अपने यात्रा वृतांत में बजहा जंगल के पास स्थित मथला गांव में गौतम बुद्ध द्वारा गांववालों को अपनी झोली से धान देने का उल्लेख किया है। आज भी बजहा गांव एवं पिपरहवा के बीच यह धान उगाया जाता है। पिपरहवा नेपाल के लुंबिनी से महज 15 किलोमीटर दूर है। लुंबिनी वही स्थान है जहां 1896 में अशोक कालीन स्तम्भ मिला था। माना गया कि वही गौतम बुद्ध की जन्मस्थली था।
कालानमक धान को लेकर शुरू हुआ अनुसंधान
एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन के अनुसार, कालानमक चावल के संरक्षण का प्रयास सबसे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। बर्डपुर, अलीदापुर एवं मोहना के जमींदार विलियम पेपे, जेएच हम्फ्रे एवं एडकन वॉकर ने इसकी अगुवाई की थी। उन्होंने ही आज के सिद्धार्थनगर जिले में कालानमक की खेती में इस्तेमाल होने वाले पानी की आपूर्ति के लिए जलाशयों का निर्माण कराया था। इन जलाशयों से पूरे साल पानी की आपूर्ति होती रहती थी। अंग्रेज खुद के खाने के अलावा दूसरे देशों में निर्यात के लिए कालानमक की खेती कराते थे। सिद्धार्थनगर के अलावा आसपास के जिलों, जैसे गोरखपुर, बस्ती आदि में इसकी खेती होती थी और यहां से यह चावल राप्ती नदी से कोलकाता तक भेजा जाता था, जहां से उसे ढाका पहुंचाया जाता था।
कालानमक धान के सतत् अनुसंधान में लगे गोरखपुर स्थित पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन (पीआरडीएफ) संस्था के अध्यक्ष डॉ. चौधरी बताते हैं, ‘किसान परिवार से होने के कारण मैंने बचपन से हमारे खेतों में कालानमक धान की उपज होते देखा था। 35 वर्ष से भी ज्यादा समय देश-विदेश में कार्य करने के पश्चात् जब अपने घर गोरखपुर लौटा, तो मालूम पड़ा कि हमारे ही गांव से कालानमक धान विलुप्त हो गया है। ये वर्ष1988 की बात है। तब हमारी संस्था ने इस दिशा में अनुसंधान करना शुरू किया। सिद्धार्थनगर में एक बैठक की गई, जिसमें करीब 200 किसान उपस्थित थे। हमारी टीम ने धान के 250 जर्मप्लाज्म (धान के नमूने) जुटाए और उनका राज्य सरकार की प्रयोशालाओं में परीक्षण किया गया। वे सभी नमूने एक-दूसरे से अलग थे। सिर्फ एक चावल के गुण उस चावल के गुण के समान मिले, जो पिपरहवा में गौतम बुद्ध के अवशेष के साथ मिले थे। यह चावल मथला गांव के फूलचंद नामक किसान से प्राप्त हुआ था।‘ मथला गांव उस बजहा गांव से करीब दो किलोमीटर दूर है, जहां गौतम बुद्ध ने प्रसाद के रूप में ग्रामीणों को धान के कुछ दाने दिए थे। फूलचचंद के पूर्वज खेती से जुड़े थे। वे अंग्रेजों के लिए भी खेती करते रहे थे। डॉ. राम एवं उनकी टीम ने उसी चावल को शुद्ध करने का निर्णय लिया। इसके बाद जो पहली प्रजाति मिली, उसका नाम पड़ा- ‘कालानमक-3’ अथवा ‘केएन3’। इसका पौधा ढाई मीटर लंबा होता है और यह तराई क्षेत्र में उगाया जाता है। 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार वने इसे जारी किया, जिसके बाद 2010 में भारत सराकर ने इसे नोटिफाई किया। किसानों एवं लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि स्वाद एवं सुगंध तो वापस आ गए हैं। लेकिन कम पैदावर की शिकायत कायम रही।
एक एकड़ में 20 क्विंटल चावल की पैदावार
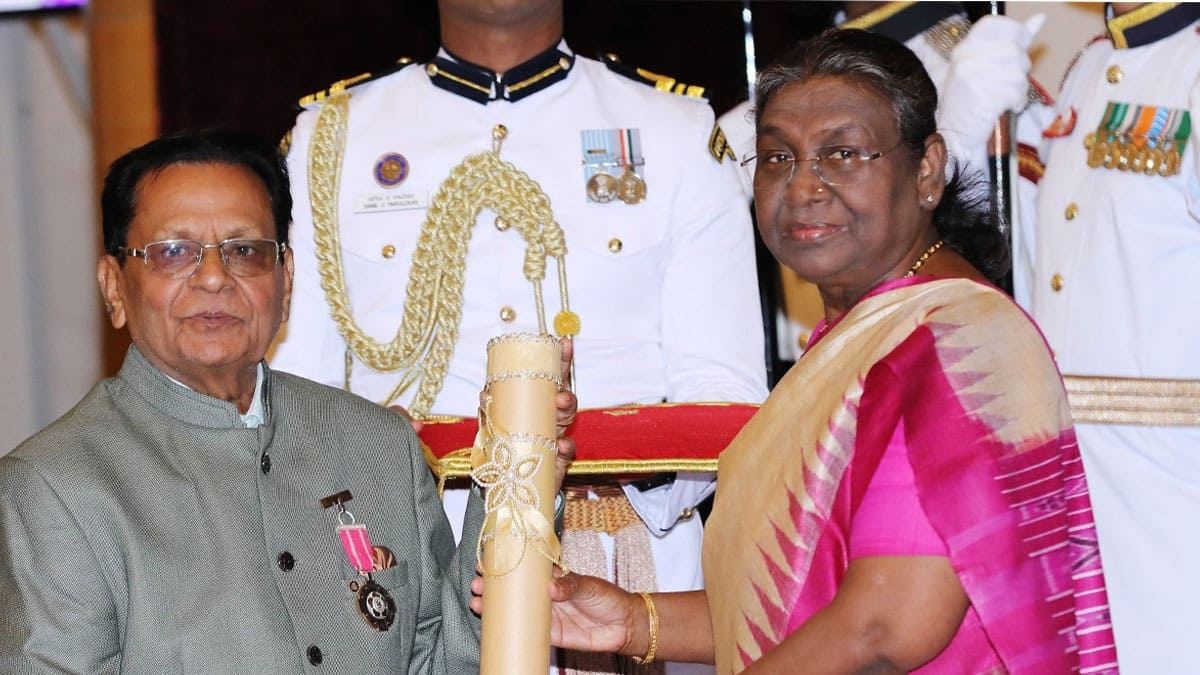
बताते हैं कि एक एकड़ भूमि में सिर्फ 10 क्विंटल कालानमक धान की पैदावार होती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉ. राम चेत चौधरी ने ‘केएन3’ वेराइटी का सांभा मसूरी चावल के साथ क्रॉस किया और उससे धान की दो अन्य बौना वेराइटी तैयार की। नई वेराइटी की ऊंचाई पुरानी ‘केएन-3’ से करीब एक मीटर से कम थी। इससे हाई इल्ड वेराइटी के बराबर इसकी पैदावार होने लगी अर्थात् एक एकड़ में अब 20 क्विंटल से अधिक कालानमक धान की उपज होती है। वे बताते हैं, ‘हमने धीरे-धीरे इसकी गुणवत्ता में और सुधार किया और 2019 में ‘कालानमक किरण’ नामक चावल रिलीज की, जो सर्वश्रेष्ठ वेराइटी है और सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। आज के समय में 80 हजार हेक्टेयर भूमि मेम इसकी खेती हो रही है यानी करीब 40 गुणा की बढ़ोत्तरी हुई है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती समेत 11 जिलों में कुल चार प्रजातियों, ‘केएन-3’, ‘बौना कालानमक 101’, ‘बौना कालानमक 102’ एवं ‘कालानमक किरण’ की खेती हो रही है। इसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल में कालानमक किरण उपजाया जा रहा है।‘ कालानमक धान की फसल को तैयार होने में 145 से 150 दिन का समय लगता है। चाहे इसे मई, जून या जुलाई में लगाएं, पहली बाली सूर्य के दक्षिणायन होने के बाद ही निकलती है। ये किसान पर निर्भर करता है कि वह कब खेतों में इसकी बुआई करता है। जहां तक पानी की आवश्यकता की बात है, तो किसी भी अन्य धान की तरह ही इसमें खाद एवं पानी का इस्तेमाल होता है। वैसे, जलजमाव वाले क्षेत्र मुफीद माने जाते हैं। अच्छी बात ये है कि नई प्रजाति के कालानमक फसल से किसानों की आमदनी पहले की अपेक्षा तीन गुणा बढ़ गई है। उन्हें चार हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर से कीमत मिल रही है। अमेजन जैसे प्लैटफॉर्म पर कालानमक चावल की बिक्री हो रही है। 2013 में कालानमक को जीआई टैग भी मिल गया। आज विदेशों में इसका निर्यात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के वन प्रोजेक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट परियोजना से भी काफी लाभ मिला है।
कालानमक धान प्रमोशन बोर्ड बनाने पर जोर
बताते हैं कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में जहां-जहां कालानमक की जैविक खेती हो रही है, उसमें सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। पीआरडीएफ (PRDF) संस्था के अध्यक्ष डॉ. आर.सी. चौधरी कहते हैं, ‘हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। उनसे नमूने इकट्ठा करवाकर उसका परीक्षण कराया जाता है। इसके अलावा नाबार्ड का भी सहयोग मिल रहा है। कुशीनगर जिले में कालानमक की प्राकृतिक खेती की जा रही है। इसमें 100 किसान शामिल हैं। आगे चलकर इनकी संख्या 150 करने की उम्मीद है। इसके अलावा, आने वाले समय में हमारी कोशिश ‘कालानमक प्रमोशन बोर्ड’ बनाने की है, जिसका मुख्यालय सिद्धार्थनगर या गोरखपुर में हो। एक बार बोर्ड बन जाने पर विदेशों में बाजार तलाशा जा सकेगा। हम कालानमक की गुणवत्ता का बेहतर ध्यान रख सकेंगे। उसकी मिलावट को रोक सकेंगे। मिलावट करने वालों को पकड़ना भी आसान होगा। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में जैविक खेती के जरिये भी इसका उत्पादन किया जाए।‘